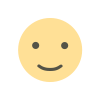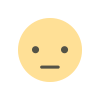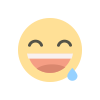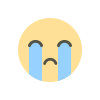हे माननीय! आप खुद ही बता दीजिए कि विगत लगभग आठ दशकों की आपकी खता क्या-क्या है? जानना चाहते हैं लोग!
चाहे संसद हो या सर्वोच्च न्यायालय, 'निर्जीव' भारतीय संविधान के ये दो 'सजीव' पहरेदार अब खुद ही श्वेत पत्र जारी करके आमलोगों को बता दें कि विगत लगभग आठ दशकों की नीतिगत लापरवाहियों और प्रशासनिक-न्यायिक विफलताओं के लिए आखिर कौन-कौन और कितना-कितना जिम्मेदार है? क्योंकि तमाम तरह की नीतिगत उलटबांसियों की अब हद हो चुकी है, देशवासी निरंतर असुरक्षित होते जा रहे हैं और वीवीआइपी सुरक्षा से लैस लोगों को हर जगह तंगहाली नहीं, हरियाली दिखाई दे रही है। इसलिए अब भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग बनाए रखने की जिम्मेदारी किसी को भी और अधिक नहीं दी जा सकती है!दरअसल, देशवासियों को यह जानने-समझने का हक है कि आखिर पूरे देश में समान मताधिकार की तरह राष्ट्रीय कानूनी और सामाजिक-आर्थिक समानता स्थापित करने और जाति-धर्म-भाषा-क्षेत्र-लिंग-वर्ग भेद मुक्त धर्मनिरपेक्ष व समतामूलक समाज बनाने की दिशा में इन दोनों संस्थाओं का क्या और कितना-कितना योगदान है? वहीं, यक्ष प्रश्न यह भी है कि क्या अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अत्यंत पिछड़े वर्गों, जातीय-भाषाई-धार्मिक अल्पसंख्यकों, गरीब सवर्णों के लिए अलग-अलग कानून बनाने की सोच निरर्थक नहीं है और धर्मनिरपेक्ष भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रशासनिक साहस यदि हमारी संसद या सुप्रीम कोर्ट में नहीं है तो फिर उनके होने या न होने का क्या अर्थ रह जाता है?इसे भी पढ़ें: अदालतों से फटकार खाकर भी नहीं सुधर रही देश की पुलिसमसलन, एक संवेदनशील और प्रगतिशील पत्रकार के रूप में यह बात मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि भारतीय संविधान के नाम पर समस्त देश में विधि-व्यवस्था बनाए रखने और उसकी निष्पक्ष समीक्षा करने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों संस्थाओं की है, जिसके लिए इन्हें लोगों की गाढ़ी कमाई से मोटी रकम भी मुहैया करवाई जाती है। बावजूद इसके ये दोनों संस्थाएं सही और स्पष्ट बात बोलने की बजाए गोल-मटोल, द्विअर्थी और बहुमत समर्थक जनविरोधी मुगलिया और ब्रितानी दृष्टिकोण को आजाद भारत में आगे बढ़ा रही हैं, जिसे कोई भी दूरदर्शी व प्रबुद्ध समाज स्वीकार नहीं कर सकता! क्योंकि सारे विवाद की जड़ वही अव्यवहारिक नीतियां हैं जो मुगलों और अंग्रेजों के अस्तित्व को खत्म करके अब शांतिप्रिय भारतीय नागरिकों के भविष्य को दीमक मानिंद चाट रही हैं? सच कहूं तो यदि इस तल्ख सच्चाई समझने की बुद्धि आपलोगों में नहीं है तो यह आईने की तरह साफ है कि इस विविधतापूर्ण देश में शासन करने योग्य आपलोग हैं ही नहीं! कड़वा सच है कि इस देश की तमाम संसदीय बहसों और तल्ख न्यायिक टिप्पणियों से वह प्रशासनिक सुधार दृष्टिगोचर नहीं हुआ है, जैसा कि भारत जैसे सुलझे हुए देश से अपेक्षा की जाती है। अब भले ही न्यायिक अतिरेक की प्रवृति पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गोड्डा सांसद निशिकांत दूबे, यूपी के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आदि ने सवाल उठाए हैं। इनलोगों ने जो बातें उठाई हैं, वह एकपक्षीय जरूर हैं, लेकिन हमारी दुःखती हुई रग को दबाने के लिए काफी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इस देश की न्यायिक प्रवृत्ति पर टिप्पणी कर चुकी हैं? किसी जनप्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने अधिकार किसी भी न्यायालय को देना लोकतांत्रिक मूर्खता है! संसद और मंत्रिमंडल के फैसले को पलट देना भी न्यायिक अतिरेक है। लेकिन यह नौबत भी इसलिए आई कि नेहरू से लेकर मोदी तक कोई पाकसाफ राजनेता नहीं आया। सबने जाति-धर्म-भाषा-क्षेत्र के लोकतांत्रिक नाले में डुबकी लगाई और लोकतांत्रिक गंगा स्नान का ऐलान करके सियासी मोक्ष पाने का डंका पीट दिया, क्योंकि दोबारा-तिबारा चुने गए। लेकिन जनता का दुःख-दर्द दूर नहीं हुआ। सबने पूंजीवादी हितों की पैरोकारी की, प्रशासनिक हितों को आगे बढ़ाया और आमलोगों के सुख-शांति की कतई परवाह नहीं की, अन्यथा ब्रेक के बाद दंगा, भीड़ का उन्माद, मुनाफाखोरी कहीं नजर नहीं आती। इसलिए संसदीय तानाशाही भी अस्वीकार्य है! संविधान की नौवीं अनुसूची की कोई जरूरत नहीं है। सामाजिक न्याय के नाम पर जातिगत अन्याय को बढ़ावा देना नीतिगत मूर्खता है। अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक का दृष्टिकोण प्रशासनिक अदूरदर्शिता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।सीधा सवाल है कि क्या इन्हीं सब दुर्दिन को दिखाने के लिए न्यायिक अवमानना और संसदीय विशेषाधिकारों से इन्हें लैस किया गया है? आखिर सर्वोपरि जनता की अवमानना और आमलोगों के विशेषाधिकार यानी मानवाधिकार की हर जगह उड़ रही धज्जियों के बारे में कौन सोचेगा, जरा आपलोग खुद ही अपने-अपने ठंडे दिमाग से सोचिए।ऐसे में सुलगता हुआ सवाल है कि विगत लगभग आठ दशकों की नीतिगत लापरवाहियों और प्रशासनिक-न्यायिक विफलताओं का ठीकरा यदि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका के सर पर नहीं फोड़ा जाए, तो फिर ये लोग ही सामूहिक रूप से बता दें कि आखिर इस बात का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। क्योंकि समकालीन राष्ट्रीय परिस्थिति दिन-प्रतिदिन विकट होती जा रही है। जिन बातों को लेकर 1947 में भारत विभाजन हुआ, वही बात आजाद भारत के हिस्से में पुनः उठना कितनी शर्मनाक है! क्या मुट्ठी भर नेताओं के सत्ता सुख के लिए करोड़ों देशवासियों के सुख-शांति में आग लगाई जा सकती है? लेकिन दुर्भाग्यवश यहां वही हो रहा है!एक सवाल और, जब समाजवादी लोकतंत्र को पूंजीवादी लोकतंत्र में तब्दील किया जा रहा था, तब जनमानस को जो आशंकाएं थीं, वह आज सही साबित हो रही हैं। क्या पूंजीपतियों के बेहिसाब मुनाफे के लिए आम आदमी के हितों की बलि चढ़ाई जा सकती है? लेकिन समकालीन पूंजीपतियों के गुणवत्ताहीन और मिलावटखोर जनद्रोही रूख और प्रशासनिक लीपापोती की भावना के बीच यह सवाल सबको मथ रहा है कि आखिर इसका जनहितकारी समाधान क्या है और इसे अविलम्ब निकलवाने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर जनशोषन कब और कौन सा विस्फोटक रूख अख्तियार करेगा, अब कोई नहीं जानता। ऐसी कोई नौबत न आए, इसलिए एलर्ट हो जाइए। अपने पड़ोसियों की हालत देखिए!- कमलेश पांडेयवरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

हे माननीय! आप खुद ही बता दीजिए कि विगत लगभग आठ दशकों की आपकी खता क्या-क्या है? जानना चाहते हैं लोग!
परिचय
भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि में अनुभव, पारदर्शिता और जिम्मेदारी की बातें अक्सर उठती हैं। हर भारतीय यह जानने का हक रखता है कि पिछले लगभग आठ दशकों में हमारी नीति निर्धारण की प्रक्रिया में कौन-कौन सी खताएं हुई हैं। इस समाचार लेख में हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे जिनपर माननीय नेतागण को खुद विचार करना चाहिए।
क्यों अपेक्षित है यह सवाल?
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबों की स्थिति में सुधार और शिक्षा प्रणाली की खामियां, ये सभी मुद्दे पिछले अनेक दशकों में मुख्य धारा बनी रहीं हैं। आज का युवा वर्ग ऐसे सवाल उठाता है जिससे वह जान सके कि पिछले नेताओं की लापरवाहियों ने कैसे उनकी भविष्य की समस्याओं को जन्म दिया है।
खताएँ: एक ऐतिहासिक संदर्भ
आधुनिक भारत की शुरुआत के बाद से, कई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आए, लेकिन क्या उनकी नीतियां ने देश को सशक्त बनाने में कोई ठोस कदम उठाए? विभाजन के बाद खुफिया नेटवर्क का कमजोर होना, धर्म के नाम पर भेदभाव, और सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ कुछ ऐसी खतरनाक गलियां थीं जिन्हें नजरअंदाज किया गया।
आर्थिक मुद्दों की अनदेखी
समाजवादी नीतियों का पालन करते हुए भी, उद्योगों की उपेक्षा, कृषि संकट और आमदनी के असमान वितरण की समस्या आज भी हमारे सामने हैं। पर्याप्त रोजगार प्रदान करने में असफल रहने वाले नेताओं को यह सवाल उठाने का हक नहीं है कि युवा क्यों उनका विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सुनवाई जरूरी है।
शिक्षा और स्वास्थ्य का ह्रास
शिक्षा और स्वास्थ्य पर किये गए सरकारी खर्चे में गिरावट ने हमारे समाज को और अधिक असमान बनाया है। सार्वजनिक स्कूलों का बुरा हाल, और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ने हमारी युवा पीढ़ी को संकट में डाल दिया है। क्या ये नेता सोचते हैं कि भविष्य में देश के विकास के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है?
समाधान की दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
इन समस्याओं की सही पहचान और समाधान के लिए आवश्यक है कि नेता खुद पहले अपनी खामियों को स्वीकार करें। इसके अलावा, एक ईमानदार संवाद की प्रक्रिया शुरू करना और युवा विचारों का आदान-प्रदान होना बहुत जरूरी है। युवा लोकतंत्र की रीढ़ हैं, और उनके विचारों को महत्व देना आवश्यक है।
निष्कर्ष
विगत आठ दशकों में माननीय नेताओं की खाई गई खामियों का समाधान केवल उन्हीं द्वारा किया जा सकता है। यह समय है कि नेताओं को अपनी जिम्मेवारियों का आभास हो और वे अपने कार्यों के प्रति सच्चे एवं पारदर्शी बनें। इस संबंध में हर सामान्य नागरिक की आवाज को सुना जाना चाहिए।
अंत में, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में लोकतंत्र की स्थिरता और वृद्धि के लिए हम सभी जिम्मेदार रहें। इसके लिए हमेशा जागरूक रहना आवश्यक है।
For more updates, visit theoddnaari.com.