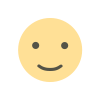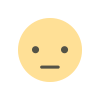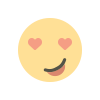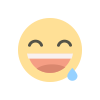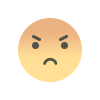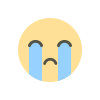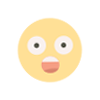हरि-हर मिलन: सनातन एकता का महादर्शन- पौराणिक, दार्शनिक और साहित्यिक प्रमाण
Hari Har Milan 2025 : सनातन धर्म की मूल अवधारणा यह है कि परम सत्ता एक (एकम् सत्) है जिसे मनीषी विभिन्न नामों से पुकारते हैं. इसी परम सत्ता की दो प्रमुख अभिव्यक्तियां हैं- विष्णु (संरक्षण और पालनकर्ता) और शिव (संहार और परिवर्तनकर्ता). यह विभाजन कार्य का है, तत्व का नहीं. The post हरि-हर मिलन: सनातन एकता का महादर्शन- पौराणिक, दार्शनिक और साहित्यिक प्रमाण appeared first on Prabhat Khabar.

–कथावाचक पं प्रदीप मिश्रा–
Hari Har Milan 2025 : भारतीय सनातन धर्म की विशालता और समन्वयवादी चेतना का उत्कृष्टतम प्रतीक यदि कोई है तो वह हरि (विष्णु) और हर (शिव) की एकात्मता है. इस मिलन को केवल दो देवताओं का संयोग मानना अपर्याप्त होगा. वास्तव में यह सृष्टि के पालन (सत्) और लय (चित्) के सिद्धांतों का अद्वैतवादी दर्शन है. यह महादर्शन पौराणिक कथाओं, भक्तिकालीन साहित्य और धार्मिक अनुष्ठानों में गहराई से समाया हुआ है. इस हरि-हर मिलन की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति चातुर्मास की अवधि और विशेष रूप से उज्जैन और काशी (वाराणसी) में मनाई जाने वाली बैकुंठ चतुर्दशी की कथाओं में निहित है.
1.हरि-हर मिलन का दार्शनिक आधार: समन्वय की सनातन चेतना
सनातन धर्म की मूल अवधारणा यह है कि परम सत्ता एक (एकम् सत्) है जिसे मनीषी विभिन्न नामों से पुकारते हैं. इसी परम सत्ता की दो प्रमुख अभिव्यक्तियां हैं- विष्णु (संरक्षण और पालनकर्ता) और शिव (संहार और परिवर्तनकर्ता). यह विभाजन कार्य का है, तत्व का नहीं.
भारतीय दर्शन में इन दो स्वरूपों की एकता को ‘हरिहरात्मक’ कहा जाता है. हरिहर एक ही विग्रह के रूप में पूजे जाते हैं. जहां एक ओर विष्णु के शांत, पीताम्बरधारी रूप का तो दूसरी ओर शिव के रौद्र, भस्मधारी रूप का चित्रण होता है. यह स्वरूप स्पष्ट करता है कि जहां सृष्टि के लिए पालन आवश्यक है, वहीं पुराने के संहार और नए के सृजन के लिए परिवर्तन (शिव तत्व) भी उतना ही अनिवार्य है. यह द्वैत कार्य-कारण का है, परंतु मूल तत्व में दोनों अभिन्न और एकाकार हैं.
यह दर्शन शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच शताब्दियों तक चले वैचारिक संघर्ष को समाप्त करने में निर्णायक सिद्ध हुआ. हरि-हर की इस एकता को स्थापित करने में भक्तिकाल के कवियों, विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास का योगदान अतुलनीय रहा, जिसकी विस्तृत चर्चा आगे की जाएगी. इस दार्शनिक पृष्ठभूमि के बिना, चातुर्मास और काशी की कथाओं का महत्व समझना कठिन है.
2.चातुर्मास: शिव द्वारा सृष्टि संचालन की पौराणिक कथा
चातुर्मास (चार महीने) की अवधि (आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल देवोत्थानी एकादशी तक) हरि और हर की एकात्मता का सबसे बड़ा व्यावहारिक प्रमाण है. इस कालखंड में सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी का हस्तांतरण होता है.
2.1. राजा बलि को भगवान विष्णु का वचन

चातुर्मास की कथा का मूल स्रोत श्रीमद्भागवत पुराण और पद्म पुराण में मिलता है. कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है. असुरों के पराक्रमी राजा बलि जिन्होंने अपने बल और तपस्या से स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया था, उनकी दानवीरता जगजाहिर थी. देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण (वामन) का रूप धारण किया और राजा बलि के पास दान मांगने पहुंचे. वामन ने बलि से केवल तीन पग भूमि का दान मांगा. राजा बलि ने बिना सोचे यह दान स्वीकार कर लिया. वामन ने विराट रूप धारण कर पहले पग में सम्पूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया. जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो भक्त बलि ने अपना मस्तक वामन के चरणों में अर्पित कर दिया.
बलि की इस अद्वितीय भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने को कहा. बलि ने विनम्रतापूर्वक वरदान मांगा- “हे प्रभु! जिस प्रकार आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया उसी प्रकार मैं आपको हमेशा अपने पास देखना चाहता हूं. आप चातुर्मास (चार महीने) की अवधि में मेरे पाताल लोक स्थित निवास में विश्राम करें.” भक्त के वश में होकर, भगवान विष्णु ने यह वचन स्वीकार कर लिया. इस वचन के पालन के लिए, भगवान विष्णु हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी (देवशयनी एकादशी) से कार्तिक शुक्ल एकादशी (देवोत्थानी एकादशी) तक योगनिद्रा में पाताल लोक में निवास करते हैं.
विभिन्न विषयों पर एक्सप्लेनर और विशेष आलेख पढ़ने के लिए क्लिक करें
2.2. भगवान शिव का उत्तरदायित्व
भगवान विष्णु को जगतपालक कहा जाता है. उनके योगनिद्रा में जाने पर सृष्टि का पालन कार्य रुकना नहीं चाहिए. इसलिए यह परंपरा स्थापित हुई कि इन चार महीनों के दौरान सृष्टि के संचालन का सम्पूर्ण दायित्व देवों के देव महादेव (शिव) ग्रहण करते हैं. इस प्रकार विष्णु के विश्राम काल में शिव पालक और संरक्षक की भूमिका निभाते हैं. यह ‘हरि-हर समन्वय’ का व्यावहारिक और अनुकरणीय उदाहरण है जहां एक देवता के विश्राम में दूसरा बिना किसी अहंकार के कार्यभार संभाल लेता है. यही कारण है कि चातुर्मास, जिसमें श्रावण मास भी आता है, शिव उपासना का सर्वोत्कृष्ट समय माना जाता है.
- काशी की कथा: बैकुंठ चतुर्दशी और सर्वोच्च भक्ति का प्रमाण
हरि-हर मिलन की सबसे भावनात्मक और गूढ़ कथा काशी (वाराणसी) से जुड़ी है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में विस्तार से मिलता है. यह कथा बैकुंठ चतुर्दशी (कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी) के महात्म्य को स्थापित करती है.
3.1. कमल-नयन विष्णु का समर्पण
जब कार्तिक मास में देवोत्थानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं तो वे सर्वप्रथम सृष्टि का कार्यभार संभालने के लिए भगवान शिव से मिलने उनकी प्रिय नगरी काशी आते हैं.
मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के पश्चात् भगवान विष्णु ने देवाधिदेव काशी विश्वनाथ का पूजन करने का संकल्प लिया. उनका संकल्प एक हज़ार (1000) स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करने का था. अभिषेक के बाद जब भगवान विष्णु पुष्प अर्पित करने लगे तब भगवान शिव ने अपने प्रिय भक्त की भक्ति की गहराई और निष्ठा को परखने के लिए एक कमल पुष्प को लुप्त कर दिया.
भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए पूरे 1000 पुष्प चढ़ाने थे. एक पुष्प की कमी देखकर वे चिंतित हुए परन्तु उनके संकल्प की दृढ़ता में कोई कमी नहीं आई. उन्होंने तुरंत विचार किया: “मुझे ‘पुंडरीकाक्ष’ (कमल जैसे नेत्रों वाला) और ‘कमल-नयन’ कहा जाता है. मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं.”
यह विचार करते ही भगवान विष्णु ने बिना किसी हिचकिचाहट या संकोच के उस एक पुष्प की कमी पूरी करने के लिए अपनी कमल-समान आंख निकालकर शिवलिंग पर अर्पित करने की तैयारी कर ली.
3.2. सुदर्शन चक्र और बैकुंठ का वरदान
भगवान विष्णु के इस अलौकिक प्रेम और सर्वस्व समर्पण को देखकर भगवान शिव तत्काल शिवलिंग से प्रकट हो गए. उन्होंने प्रेम से विष्णु को रोक लिया और गदगद होकर कहा, “हे विष्णु! तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है. तुम्हारा यह समर्पण, भक्ति और निष्ठा अतुलनीय है.”
शिव ने प्रसन्न होकर विष्णु को उनके सर्वाधिक शक्तिशाली और अलौकिक अस्त्र सुदर्शन चक्र भेंट किया, जिससे वे धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार कर सकें. साथ ही, उन्होंने यह महावरदान दिया कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का यह पावन दिन ‘बैकुंठ चतुर्दशी’ कहलाएगा. इस दिन जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक हरि (विष्णु) और हर (शिव) का एक साथ पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी और उसके जन्म-मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा. यह कथा हरि-हर की एकात्मता के साथ ही भक्ति की पराकाष्ठा को भी दर्शाती है. यहां साध्य और साधन में कोई भेद नहीं रह जाता. - साहित्यिक प्रमाण और गोस्वामी तुलसीदास का योगदान
हरि-हर एकता का विचार केवल पुराणों तक सीमित नहीं रहा. इसे भक्तिकाल के साहित्य ने जन-जन तक पहुंचाकर एक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया.
4.1. गोस्वामी तुलसीदास (भक्तिकाल के सेतु)
गोस्वामी तुलसीदास जी (16 वीं शताब्दी) का योगदान इस संदर्भ में अप्रतिम है. उनके समय में शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच मतभेद अपने चरम पर था, जो सामाजिक वैमनस्य का कारण बन रहा था. तुलसीदास जी स्वयं श्रीराम (विष्णु अवतार) के अनन्य भक्त थे फिर भी उन्होंने अपने महाकाव्य ‘रामचरितमानस’ के माध्यम से शिव और राम (विष्णु) की अभिन्नता को स्थापित किया.
तुलसीदास जी ने शिव को राम का और राम को शिव का परम आराध्य बताया. रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं:
“सिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा.”
(अर्थात्: जो शिव का द्रोही होकर भी मेरा भक्त (दास) कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता.)
यह एक अकेली चौपाई विष्णु भक्तों के लिए शिव-पूजा को अनिवार्य बना देती है और संप्रदायों के बीच की वैचारिक खाई को पूरी तरह पाट देती है. उन्होंने शिव को राम-कथा का प्रथम वक्ता (सती को रामकथा सुनाते हुए) और विष्णु को शिव का परम स्तुति-गायक (शिव-विवाह में) चित्रित किया. तुलसीदास ने सिद्ध किया कि दोनों की पूजा एक-दूसरे को प्रसन्न करने का माध्यम है न कि प्रतिद्वंद्विता का विषय.
4.2. अन्य शास्त्रीय प्रमाण
स्कंद पुराण: इसमें स्पष्ट उल्लेख है: “यथा शिवस्तथा विष्णुर्यथा विष्णुस्तथा शिव:. अन्तरं शिव विष्णोश्च मनागपि न विद्यते.” (जैसा शिव हैं, वैसे ही विष्णु हैं; शिव और विष्णु में रत्ती भर भी अंतर नहीं है).
आदि शंकराचार्य: अद्वैत वेदांत के महान प्रवर्तक आदि शंकराचार्य (8 वीं शताब्दी) ने अपने “हरिहरात्मक स्तोत्रम्” में दार्शनिक एकता का स्पष्ट उल्लेख किया.
विष्णु पुराण: यह वैष्णव पुराण भी शिव-विष्णु की अभिन्नता को विभिन्न कथाओं और स्तुतियों के माध्यम से पुष्ट करता है.
5.लोक परम्परा:
काशी की देव दिवाली: बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि-हर मिलन की खुशी में, देव लोक में भी दिवाली मनाई जाती है, जिसे देव दिवाली कहा जाता है. इस दिन देशभर में नदी घाटों पर दीये जलाए जाते हैं. यह शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं के भक्तों द्वारा एक साथ मनाया जाने वाला अनुष्ठान है.
उज्जैन की यात्रा (शोभायात्रा): भगवान महाकाल का पालकी में सवार होकर गोपाल मंदिर तक जाना एक सांस्कृतिक शोभायात्रा का रूप ले लेता है, जिसमें भजन-कीर्तन, स्थानीय संगीत और लोक-नृत्य शामिल होते हैं. यह धार्मिक अनुष्ठान को एक व्यापक सांस्कृतिक महोत्सव का रूप देता है, जहाँ आस्था और कला का मिलन होता है.
सीहोर का हरि-हर मिलन: कुबेरेश्वर धाम में स्थापित कुबेरेश्वर महादेव (हर) और मुरली मनोहर (हरि) के मिलन के भव्य समारोह में पूरे देश से श्रद्धालु एकत्रित होते हैं. स्थानीय लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए धाम के समारोह में सम्मिलित होते हैं. - आधुनिक संदर्भ और कुबेरेश्वर धाम का योगदान
हरि-हर मिलन की इस प्राचीन परंपरा को वर्तमान समय में भी विभिन्न संतों और कथावाचकों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है. सीहोर के कुबेरेश्वर धाम ने लोक कलाओं को हरि-हर एकता के एक विशाल जन-मंच के रूप में स्थापित कर इस परंपरा को लाखों भक्तों तक पहुंचाया है.
संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के समन्वयवादी सिद्धांत हमारे मार्गदर्शक रहे हैं. जब भारतीय समाज अपने सबसे संकट के दौर से गुजर रहा था ऐसे समय में गोस्वामी जी ने अपने विचार और संदेश के माध्यम से समाज के आपसी मतवैभिन्न को समाप्त कर मूल एकता और सरलता पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया. हमारे उपाय भी लोगों को धर्म की मूलभूत एकता से जोड़ते हैं और कठिन अनुष्ठान के व्यय और जटिलता से मुक्त करते हैं. - पं. मिश्रा द्वारा बताए गए हरि-हर मिलन के उपाय और उसके दार्शनिक निहितार्थ
तुलसी-बेलपत्र शहद का महा-उपाय बेलपत्र (शिव को प्रिय) और तुलसी दल (विष्णु को प्रिय) को एक साथ प्रयोग करना ही हरि-हर का मिलन है. यह उपाय स्पष्ट करता है कि शिव-भक्त को तुलसी और विष्णु-भक्त को बेलपत्र को सम्मान देना चाहिए.
दीपदान का महत्व इस दिन 14 दीपक घर के मंदिर, चौखट, और विशेष रूप से आंवला (विष्णु प्रिया) तथा बेलपत्र (शिव प्रिया) वृक्षों के नीचे दान किए जाते हैं. इससे प्रकृति की मूल एकता और तादात्म्य प्रदर्शित होता है.
रोग-मुक्ति का जल-अर्पण दूध और पाँच बेलपत्र मिश्रित जल को शिवलिंग या पीपल वृक्ष (विष्णु स्वरूप) की जड़ में अर्पित करना तथा {ॐ ह्रीं ॐ हरिणाक्षाय नमः शिवाय} मंत्र का जाप करना. यह मंत्र स्वयं में हरि (हरिणाक्ष) और हर (शिवाय) का संयुक्त नाम है.
इन अनुष्ठानों के माध्यम से कुबेरेश्वर धाम ने हरि-हर एकता को पूजा-पद्धति का अनिवार्य अंग बना दिया है, जिससे सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता की भावना मजबूत हुई है.
उपसंहार
हरि-हर मिलन सनातन धर्म का वह शाश्वत सत्य है, जो हमें सिखाता है कि सृष्टि में कोई भी शक्ति या सिद्धांत एक-दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक है. चातुर्मास की कथा सृष्टि के कार्यभार के सहयोगपूर्ण हस्तांतरण की बात करती है, तो काशी की कथा भक्ति की पराकाष्ठा और प्रेम के माध्यम से प्राप्त होने वाले मोक्ष की ओर इशारा करती है. गोस्वामी तुलसीदास ने इस दार्शनिक सत्य को कविता की सरलता से जन-मानस तक पहुँचाया. वर्तमान समय में इसे शास्त्र और पुराण से निकाल कर लोक के मध्य स्थापित करने का कार्य कुबेरेश्वर धाम कर रहा हैं.
अंततः हरि-हर मिलन केवल मंदिर की मूर्ति या कथा का विषय नहीं है. यह जीवन का दर्शन है जो हमें द्वेष और मतभेद से ऊपर उठकर समन्वय, सहयोग और एकात्मता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है. यही सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी थाती है—एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का भाव.
ये भी पढ़ें : Chhath Puja 2025 : छठ महापर्व में पंडित-पुजारी की जरूरत नहीं, मन के भाव से होती है कठिन व्रत की पूजा
The post हरि-हर मिलन: सनातन एकता का महादर्शन- पौराणिक, दार्शनिक और साहित्यिक प्रमाण appeared first on Prabhat Khabar.